योगक्षेमं
वहाम्यहम्
यूँ तो श्रीमद्भगवद्गीता के प्रत्येक
संदेश अपने आपमें अद्भुत हैं, फिर भी कुछेक संदेशों को विशिष्ट की श्रेणी में रखने
को मन मचल उठता है। उन्हीं में एक है श्रीकृष्ण का ये प्रतिज्ञात्मक-आश्वासनात्मक
अद्भुत संदेश—
अनन्याश्चिन्तयन्तो
मां ये जनाः पर्युपासते ।
तेषां
नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ।। (९।२२)
गगन-गम्भीर श्रीकृष्ण चपलता
के लिए भी सुप्रसिद्ध हैं। यही कारण है कि इससे पूर्व, अध्याय ४-११
में बड़ी चतुराई पूर्वक कह चुके हैं—ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव
भजाम्यहम् ।। (जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार शरण
देता हूँ।)
नये विचार वाले कह सकते हैं
कि ये तो ‘tit
for tat’ – ‘जैसे को तैसा’
वाली बात हो गयी। ये ‘यथा-तथा’
वाला गुण तो सामान्य मनुष्य वाली मानसिकता हो गयी। फिर आम आदमी और श्रीकृष्ण में
अन्तर ही क्या रह गया !
किन्तु यही सोचकर हम उलझ
जाते हैं। फँस जाते हैं—मायापति की मायाजाल में— दुनियादारी में।
अद्वैतवादी मानते हैं कि
ब्रह्म का ही नानाविध स्वरुप (विस्तार) है समस्त ब्रह्माण्ड। यानी कि ब्रह्म के
सिवा और कुछ है ही नहीं।
फिर किसे फँसना, किसे फँसाना?
यानी जो कुछ है उसी एक,
मायापति का लीला-विलास है।
और, एक बात तो सुनिश्चित है
कि कर्म का कठपुतला है प्राणी—कर्मण्येवाधिकारस्ते...(२-४७)
। कर्म करने मात्र का अधिकार है उसके पास। फल—कितना, क्या, कब, कहाँ के बारे में
कुछ अता-पता नहीं उसे।
किन्तु ये भी सत्य है कि भोग
की चाह होगी तो भोग मिलेगा, योग की सतत चाह होगी तो योग-लब्ध होगा । किन्तु ऐसा भी
नहीं है कि जिस क्षण चाहेगा, उसी क्षण प्राप्ति हो ही जायेगी।
ऊपर में जो यथा-तथा
वाली बात कही गयी है—इसी संदर्भ में है। सांसारिक प्राणी-पदार्थों की कामना-पूर्ण
यजन-याजन सांसारिकता की ओर ही घसीटेगी और कृष्ण की चाह कृष्ण की ओर ही ले जायेगी। यही
अन्तर है नश्वर और अनश्वर की चाह में। इसपर बल देते हुए कृष्ण कहते हैं— नेहाभिक्रम
नाशोऽस्ति
प्रत्यवायो न विद्यते । स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ।।
(२-४०)
ये अद्भुत कर्ममार्ग है, जिसपर चल पड़ने पर कदापि प्रत्यवाय (विपरीत फल) नहीं
होता।
किन्तु ध्यान देने की बात है
कि कुछ चाहे, कि गए काम से। मांगे, कि फँसे। चतुर वो है, जो कुछ चाहत ही न रखे।
चाहत के साथ ही यथा-तथा वाली प्रतिज्ञा लागू हो जाती है।
कृष्ण का एक नाम ‘अमन’ भी है—बिना मन वाला— जिसके पास मन
हो ही नहीं। कृष्ण से भी चतुर वृन्दावन की
गोपियों ने एक बार कहा— तुम्हारे पास तो सबकुछ है ही, मन नहीं है। इसलिए हम अपना
मन तुम्हें समर्पित कर रहे हैं।
विद्वानों ने ‘मन’ को सर्वाधिक बलवान बताया है। इसे
नियन्त्रित करना सामान्य जन ही नहीं, प्रत्युत साधकों के लिए भी चुनौती-पूर्ण है।
चतुरा गोपियाँ इसीलिए अ-मन को अपना मन समर्पित करना चाह रही हैं।
अब आते हैं उस विशिष्ट संदेश
पर—योगक्षेम वहन करने वाली बात पर। कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भाव से हमें चाहता
है, उसके योगक्षेम को हम वहन करते हैं। योगक्षेम का भावार्थ है—अप्राप्त की
प्राप्ति में सहायक और प्राप्त की रक्षा में तत्पर।
जो नहीं है हमारे पास, उसे
पाने के लिए सदा वेचैनी बनी रहती है और जो है, उसकी रक्षा की भी उतनी ही वेचैनी
रहती है। धन नहीं है, तो धन पाने की व्यग्रता और प्राप्त हो जाए तो उसे सहेजने की
चिन्ता। पाने-सहेजने की चिन्ताओं के भँवर में सदा ऊँब-चूब होते, जीवन गुजर जाता
है।
सर्वविध समर्पित भक्त के लिए
भगवान यही तो करते हैं। उसे क्या, कब, कितना चाहिए सब पता है और समय पर
सुव्यवस्थित कर देता है। किन्तु इसके लिए सबसे अहम् शर्त है—अनन्यता ।
ये अनन्य क्या है?
न
अन्य अनन्य—जहाँ कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और हो ही नहीं। यही
है सर्वस्व समर्पण की स्थिति। पूर्णरुपेण समर्पण की स्थिति। बिलकुल निर्बोध बालक वाली
स्थिति, जिसे माँ की गोद में गिरने-मरने की भी परवाह नहीं होती। सवस्त्र-निर्वस्त्र
की भी परवाह नहीं होती। पतिपरायणा परिणीता की भी यही भावदशा होती है। अपने स्वामी
के समक्ष वह पूर्ण समर्पित हो जाती है। उसके शरीर और मन पर स्वामी का पूर्ण अधिकार
होता है।
इस अन्यन्यता में ही किंचित
त्रुटि थी कात्यायनी-उपासिका गोपियों में—गोपीवल्लभ कृष्ण के अतिरिक्त यमुना-पुलिन
पर उनके सामने विस्तृत संसार था। अपने आप की निर्वस्त्रता का भी भान था। लोक-लज्जा
का भ्रमजाल भी था।
और यदि ये सब उपस्थित था
ही,फिर अनन्यता का बोध कहाँ !
सामान्य जन से कृष्ण के इस
दिव्य भाव को ठीक से समझने में ही चूक हो जाती है और चीरहरण लीला को दुनियादारी
वाली आँखों से देखने लगते हैं। कृष्ण का एक मात्र उद्देश्य गोपियों की अनन्यता की
पूर्णता ही थी, कुछ और नहीं। अन्यन्यता की पूर्णता का जीता जागता प्रमाण है—रासलीला।
शत-सहस्र गोपियाँ और एक मात्र उनके गोपीवल्लभ कृष्ण। किन्तु मजे की बात ये है कि
प्रत्येक गोपी यही अनुभव कर रही थी कि कृष्ण तो सिर्फ और सिर्फ उसके बाहुपाश में
आबद्ध हैं।
कृष्ण और गोपी, गोपी और
कृष्ण—ये युगल भाव भी तो अनन्तः तिरोहित हो जाना है—अद्वैत के उत्तुंग क्षणों में
। किन्तु द्वैत इसकी अनुमति नहीं देता और चाह भी नहीं होती—तिरोहण की।
बात यहाँ हो रही है अनन्यता
की। अनन्यता के बिना योगक्षेम का बीड़ा नहीं उठाया जा सकता और अनन्यता आते ही
सबकुछ निर्वाध चलने लगता है।
गोपियों का चीरहरण और
द्रौपदी का चीरहरण—प्रथम दृष्ट्या दोनों समान क्रियायें हैं, किन्तु दोनों दो
ध्रुवों पर हैं और कुछ अर्थों में एक ही दिशा में। गोपियों का चीरहरण कृष्ण के
द्वारा ही किया गया। उनकी साधना को त्रुटिहीन करने हेतु। जबकि द्रौपदी के
चीरहरण-कुकृत्य में कृष्ण का वस्त्रावतार हो गया। किन्तु ये तबतक नहीं हुआ, जबतक
उसकी दृष्टि में राजसभा और उसके सभासद उपस्थित रहे। बाहुबली पाँच पतियों पर भरोसा रहा। फिर जरा उधर
से डिग कर, अपनी ही भुजाओं पर आ टिका रक्षा का बोध। वस्त्रावतार तो तब हुआ, जब दोनों हाथ ऊपर उठाकर सखी
कृष्णा ने सखा कृष्ण को पुकारा । इस प्रकार द्रौपदी और गोपियों की अन्तिम स्थिति
में कोई विशेष अन्तर नहीं है।
न अन्य अनन्य—इसे ही कहते
हैं।
किन्तु ये मनस्थिति, ये भावस्थिति
आजीवन नियमन-संयमन के पश्चात ही लब्ध हो सकती है। ये कोई स्कूली पाठ्यक्रम नहीं
है,जिसे निश्चित समय में कोई विद्यार्थी पूरा कर ले या कोई वरिष्ठ शिक्षक पूरा करा
दे । शास्त्र या गुरु सिर्फ आलोक प्रज्वलन की भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। आलोकित
मार्ग का सम्यक् दर्शन कर, पथ-गमन तो हमें स्वयं ही करना होगा ।
और सबसे बड़ी बात ये है कि
अनन्यता का आनन्द अनुभूति का विषय है। लाख
चेष्टा के पश्चात् भी शब्दों में पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। और जो
शब्दों में समाने योग्य है ही नहीं, उसे चाह कर भी कैसे व्यक्त करुँ किसीके समक्ष? मेरी भी विवशता है।

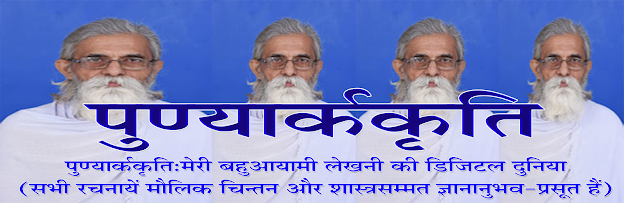
Comments
Post a Comment