विवाह : निवाह
: पुनर्विचार
सृष्टिमात्र
परमात्मस्वरूप है। एकमात्र परमात्मा अनेक रूपों
में दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे में जिज्ञासा सहज है कि परब्रह्मपरमात्मा तो
एक है, फिर उसे अनेक होने की आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई? इसका समाधान (उत्तर) बृहदारण्यक-१-४-३, तैत्तिरीय-२-६
आदि उपनिषदों में मिलता है— एकोऽहं बहुस्याम्, एकाकी न रमते, स द्वितीयमैच्छत्, स आत्मानं द्वेधा
पातयत्, पतिश्च पत्नीश्चाभवत्, सोऽकामयत बहुस्याम् प्रजायेयेति, कामं बिना
सृष्टिरेव न भवति...इत्यादि।
(एक हूँ,अनेक हो जाऊँ। एकाकी रमण नहीं हो सकता। उसने दूसरे की इच्छा की। अपने
में से ही दूसरा स्वरूप प्रकट किया। वे ही पति भी बने, पत्नी भी । उन्होंने कामना
की बहुत हो जाऊँ। काम के बिना सृष्टि नहीं हो सकती।)![]()
उक्त
वचनों पर विचार करने पर लगता है कि परमात्मसृष्टि का सर्वाधिक संवेदनशील
विषय है काम (इच्छा, कामना) और इसे ही सृष्टि का बीज भी कहना चाहिए। इस ‘एक से अनेक हो जाऊँ’ की ऐष्णा ने ही कालान्तर में
विवाह-परम्परा को जन्म दिया। सृष्टि के प्रारम्भिक काल में तो ऐसी स्थिति
(व्यवस्था) थी कि सहज रूप से एक से अनेक का सृजन सम्भव होते गया। किन्तु ये
व्यवस्था बहुत आगे तक चली नहीं। सम्भवतः इसे चलने देना भी नहीं चाहा गया ।
परिणामतः दक्षिण-वाम भागों से क्रमशः पुरुष और स्त्री नामक दो स्वरूपों का सृजन
हुआ, जिनकी कायिक संरचना और क्रिया-कलापों में यत्किंचित् भेद भासित है। इसी भेद
को पुनः अभेद की स्थिति में पहुँचाने का उपक्रम ही विवाह-व्यवस्था है। वस्तुतः
पुरुषार्थ चतुष्टय—धर्म, अर्थ, काम के पश्चात् मोक्ष (विलय)(अभेद) की स्थिति को
लब्ध होना, विवाह-व्यवस्था की अन्तिम परिणति है।
यही कारण है कि सनातन संस्कृति में विवाह को अति महत्त्वपूर्ण धार्मिक
संस्कार माना गया है। पति-पत्नी के सम्बन्ध को आध्यात्मिक सम्बन्ध कहने में कोई
आपत्ति नहीं होनी चाहिए। धर्माविरुद्ध (धर्म के अविरुद्ध) काम का सेवन करते हुए
प्रजोत्पत्ति और गृहस्थधर्म का सम्यक् पालन ताकि त्रि-ऋण (देव, ऋषि, पितृ) से
निवृत्त होकर, पुनः अनेक से एक की ओर सहज गमन सम्भव हो सके—यही तो अभीष्ट है विवाह
का। सुदीर्घ ब्रह्मचर्य के पश्चात् वेदाध्ययन-समावर्तनसंस्कारों के बाद
गृहस्थाश्रम में प्रवेश की अनुमति मिलती है। जहाँ प्रजोत्पत्ति से प्रजापालन तक
कर्मों का सम्यक् निर्वहण करते हुए, मोक्षमार्ग की ओर अग्रसर होने की पूरी
स्थितियाँ बनायी जाती हैं।
सनातन मार्ग से दिग्भ्रमित जन
वैवाहिक मर्यादाओं से च्युत होकर, भोगेष्णा में संलिप्त रह जाते हैं और उनकी समझ
से विवाह का यही अथ और इति सिद्ध होता है; जबकि भोग से
संतृप्त होकर, मोक्ष की ओर गमन, मानव का लक्ष्य होना चाहिए।
ध्यातव्य है कि स्त्री भोग्या नहीं
है। पुरुष भोक्ता नहीं है। वस्तुतः सृष्टियान के ये दो चक्र हैं, जिन्हें अपने परम
लक्ष्य को लब्ध करने में निरन्तर प्रयासरत रहना है।
गृहस्थआश्रम को सभी आश्रमों का
उपकारक कहा गया है। चारो आश्रमों के मूल में यही आश्रम है—चत्वारः आश्रमाः
प्रोक्ताः सर्वे गार्हस्थ्यमूलकाः। यही कारण है कि इसे तीनों आश्रमों की योनि
भी कहा गया है— त्रयाणामाश्रमाणां तु गृहस्थो योनिरुच्यते। (दक्षस्मृति २-४८)
तथा वशिष्ठस्मृति ८-१६ में इन्हीं भावों को किंचित् अन्य शब्दों में व्यक्त किया
गया है— यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः। तथा गृहाश्रमं प्राप्यं सर्वे
जीवन्ति चाश्रमाः।। अतः मनुस्मृति ४-१ के वचन— चतुर्थमायुषो
भागमुषित्वाद्यं गुरौ द्विदः। द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्— का पालन करते हुए आयु के दूसरे
चतुर्थांश में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की अनुशंसा की जाती है। क्योंकि गृहवासो
सुखार्थो हि पत्नीमूलं च तत्सुखम्। (दक्षस्मृति ४ ) (गृहस्थाश्रम के मूल में पत्नी
(गृहणी) है— न गृहं गृहमित्याहुर्गृहणी गृहमुच्यते। (गृहणी के होने से ही
गृह संज्ञा है)। गृहणी को धर्मपत्नी भी कहते हैं, यानी कोई भी धार्मिककृत्य इसके
सहयोग-सानिध्य बिना असम्भव है। अपूरित है। वस्तुतः ये सहधर्मिणी है, अर्द्धांगिनी
है—स्त्री-पुरुष मिलकर ही पूर्णांग होता है। इसके बिना दोनों ही अपूर्ण हैं। मनुस्मृति
९-१०१,१०२ में निर्दिष्ट है—
अन्योन्यस्याव्यभिचारो
भवेदामरणान्तिकः।
एष धर्मः समासेन ज्ञेयः
स्त्रीपुंसयोः परः।।
तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसौ तु
कृतक्रियौ।
यथा नाभिचरेतां तौ
वियुक्तावितरेतरम्।। (पति-पत्नी दोनों का जीवनपर्यन्त धर्म,अर्थ,काम के विषय में व्यभिचार न हो,
अर्थात् त्रिवर्ग साधन में पार्थक्य न हो। दोनों अपनी मर्यादा में स्थित होकर
कर्मानुष्ठान करें। )
ध्यातव्य है कि इस
प्रकार का गरिमामय विवाहसंस्कार हमारे सनातन संस्कृति में ही है, अन्यत्र नहीं।
किन्तु अब से कई दशक पहले जे. बी. वाटसन नामक एक समाजशास्त्री ने
प्रश्न चिन्ह लगाया था हमारी इस आध्यात्मिक व्यवस्था पर— ‘‘क्या विवाह संस्था
अगले ५० बर्षों बाद भी जीवित रह सकेगी?’’
‘हस्तिपादतलदृष्टि’ वालों
ने इसे धार्मिकसंस्कार नहीं, बल्कि संस्था मान लिया। विवाहसंस्कार को
अपने-अपने ढंग से दुनिया ने परिभाषित कर लिया। आध्यात्मिक प्रेमोदधि में छलांग
लगाने वाली व्यवस्था, सामाजिक समझौते वाले क्षुद्र गर्त में औंधे मुँह गिर पड़ी।
विवाह ‘निर्वाह’ बन गया। जबतक निभे निभावो, न निभे हटाओ। ‘अंग’
‘परिधान’ बन गया। कपड़ों की तरह
पति-पत्नी बदले जाने लगे। ये परिवर्तन ही सभ्यता का प्रमाण हो गया।
सुदीर्घ पराधीनता के पश्चात् स्वतन्त्र भारत में मई १९५५ई. में
हिन्दू विवाह अधिनियम जब थोपा गया हमारे ऊपर, तब से हमारे इस परम पावन संस्कार पर
भी ग्रहण लग गया। म्लेच्छानुकरण करते हुए तथाकथित वैधानिक सींकचे में जकड़कर, धातक
कर्तनी से वैदिक विवाह का भी विच्छेद कराया जाने लगा है और हम उसे सामाजिक रूप से
स्वीकारने भी लगे हैं। हम ये भूल गए हैं कि जिसने जोड़ा नहीं है, उसे तोड़ने का
अधिकार भी नहीं है। विवाह ‘मैरेज़’ नहीं है, जिसमें ‘डायवोर्स’ हो जाये कानूनी सलाह से। स्पष्ट है
कि जिस कानून ने मैरेज कराया है, वो कानून उसे तोड़ने पर भी विचार कर सकता है।
किन्तु जिसे कराया ही नहीं, उसे तोड़ने वाला वो कौन होता है—सोचने वाली बात है।
विवाहसंस्कार अदालती विषय नहीं है।
यहाँ कठघरे वाला मिथ्या शपथ नहीं है और न निबन्धन-पंजिका पर हस्ताक्षर वाला
प्रमाणपत्र। ये तो वैदिक ऋचाओं द्वारा, अनन्त शक्तियों द्वारा, अग्नि-सूर्य की
साक्षी में बनायी गयी ग्रन्थि है, जो शरीर
ही नहीं आत्मिक तल पर लगाई गई है। इसे जन्म-जन्मान्तर तक भी खुलना कठिन है।
शरीरान्त से भी इसका नाश सम्भव नहीं। शरीर रहते भला क्योंकर नष्ट होगा ! सच्चाई ये है कि
हमारे सनातन विवाह पद्धति में विच्छेद का अनुच्छेद ही नहीं है—ये हमें जान लेना
चाहिए। विवाह परस्पर समर्पण सम्बन्ध है। ‘विलय’ ही इसकी परिणति है।
‘वि’ उपसर्ग एवम् ‘वह्’ धातु से बना
शब्द विवाह का अर्थ होता है, विशेष रुप से उठाकर ले जाना। समान
भाव-व्यंजक और भी कई शब्द हैं— ‘परिणय’ जो ‘परि’ उपसर्ग ‘नी’ धातु से बना है। इसका अर्थ है— पूरी तरह से
ले जाना। ले जाने वाले को ‘बोढ़ा’ कहते हैं। ‘पा’ रक्षणे
धातु से बना शब्द पति यानी रक्षा का दायित्व वाला और दूसरा शब्द है—‘भर्ता’ यानी भरण-पोषण करने वाला। इन भिन्न-भिन्न
अर्थ-बोधक शब्दों में भाव एक ही है। उद्देश्य भी एक ही है—कर्त्तव्यबोध । ध्यातव्य
है कि पति
परमेश्वर है यदि तो पत्नी भी देवी है।
विडम्बना ये है कि कर्त्तव्य-बोध
शनैःशनैः तिरोहित होता गया और अधिकार-बोध हावी होता चला गया। सुव्यवस्थित
धर्मशास्त्र पर कुंठित समाजशास्त्र का
वर्चश्व हो गया। फलतः ‘वर्चश्व और प्रतिस्पर्धा’ का वर्ग-संघर्ष प्रारम्भ
हो गया। पुरुष एक वर्ग बन गया, नारी एक वर्ग। एक ‘महत्’ दो ‘अहं’ हो गए। ये दो
ही तो द्वन्द है। और द्वन्द्व का परिणाम— एक ही चुम्बक के दो ध्रुवों के बीच
संघर्ष। पावन वैदिकसंस्कार प्रदूषित हो गया। दमन-शोषण जैसी सामाजिक कुरीतियाँ तेजी
से पनपने लगीं। पुत्र-पुत्री में भयंकर भेद हो गया। ‘कन्या’
न जाने कब ‘दुहिता’ हो गयी—दोहन करने वाली। दो आत्माओं, दो कुलों, दो परिवारों, दो परिवेशों
को मिलाने वाले प्रेम-सौहार्द के मण्डप में ‘दहेजदानव’ का विनाशकारी ताण्डव प्रारम्भ हो गया। दहेज की बलिवेदी पर प्रेम की
आहुतियाँ पड़ने लगी। अधिकाधिक दहेज लेना सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय हो गया। ‘अर्थ’ के सामने ‘धर्म’ बौना बन गया। वैदिककर्मकाण्ड क्रमशः सिमटते गए। आडम्बर-दिखावा विस्तार
पाता गया।
अतः भ्रष्ट कानून के कुठाराधात और मानव से दानव
होते चले जा रहे, हाथी की तरह पैरों तले दृष्टि रखने वाले समाज की इन कुरीतियों का
परिष्कार अत्यावश्यक है। विश्वगुरु आर्यावर्त को पुनः अपने सभी संस्कारों का
अध्ययन- मनन-चिन्तन करते हुए, कठोरता से पालन करने की आवश्यकता है। अस्तु।
![]()
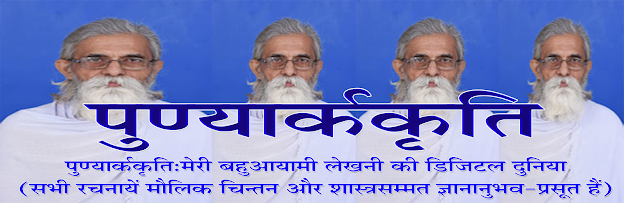
विवाह में धार्मिक और सामाजिक मर्यादाओं के सदैव पालन करते रहने की स्वीकारोक्ति भी महत्वपूर्ण होती है.विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध होता है.शारीरिक संबंध केवल वंश वृद्धि के उद्देश्य से ही होता है.मैरिटल रेप जैसी मानसिकता के लिए विवाह व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है.पतिव्रत लिए पत्नी तथा एकपत्नी व्रत लिए पति की मान्यता केवल विवाह पद्धति में ही पाई जाती है.ऐसे में, भारत का वह व्यभिचार निरोधक कानून (आईपीसी की धारा 497, जिसे एक साज़िश के तहत ख़त्म किया गया) बिल्कुल उचित था.
ReplyDeleteसाथ ही, चूंकि पति-पत्नी के बीच संबंध जन्म-जन्मांतरों का होता है इसलिए, यह अविच्छिन्न होता है, और इसे किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता है.अध्ययन से पता चलता है कि हिन्दू व्यवस्था में डिवोर्स (Divorce) और तलाक़ यानि, विवाह विच्छेद के लिए कोई शब्द ही नहीं है..https://khulizuban.com/vivah-shadi-nikah-and-marriage-are-different-in-their-meanings-and-concepts-analysis/