बाबा
वटेसरनाथ
सौभाग्य
से आँख-कान के साथ मन का घुड़दौड़ जारी हो और इनके साथ-साथ दिमाग भी दुरुस्त हो,
तो निश्चित मानिए कि चहुँओर दृश्यों और घटनाओं की बाढ़ नजर आयेंगी। संयोग से आपका
मन जरा लेखकीय ‘लत’ वाला हो तो संस्मरणों और आलेखों में कैद करने
को आकुल हो ही जायेगा।
बाबा
वटेसरनाथजी ऐसे ही एक विशेष व्यक्ति हैं, जिनके बारे में कुछ कहे-बतलाये बिना मन
बेचैन हो रहा है। किन्तु इससे पहले ये स्पष्ट कर दूँ अपने स्नेही जनों से, खासकर
उन पाठकों से, जो हमारे प्यारे “वटेसरकाका की
बतकहियों ” से बाकिफ हैं – बाबा वटेसरनाथ पुराने परिचित वटेसरकाका नहीं,
बल्कि उनसे बिलकुल भिन्न व्यक्तित्व वाले एकदम अनजान व्यक्ति हैं आप सबके लिए।
इनके बारे में जान लेने के बाद आपको भी लगेगा—कहाँ वटेसरकाका और कहाँ वटेसरनाथ !
वैसे
भी चिर परिचितों से मिलने की तुलना में नए व्यक्ति से मिलने का अलग ही आनन्द है।
अब इसका ये अर्थ आप न लगा लें कि पुराने लोगों से नहीं मिलना चाहिए।
अरे भाई ! मगही में एक कहावत है कि पथ्य
पुराने चावल का ही होना चाहिए। किन्तु नए चावल का स्वाद लेना भी कम प्रीतिकर नहीं
हुआ करता और नये चावल का भात यदि ‘मड़गिज्जा’
हो जाय तो उसका मजा ही कुछ और है— डालिए दही-चीनी और मारिए सपासप...।
अतः
आज आपको नए वाले बाबा वटेसरनाथजी से परिचय करा ही देता हूँ ।
बाबा
वटेसरनाथ मगध क्षेत्र के जानेमाने परम वैष्णव परिवार में जन्म लिए थे, जिसके घर
में प्याज-लहसुन का छिलका भी कहीं से उड़-पड़कर आ जाए तो पंचगव्य का छिड़काव पूरे
घर में करना पड़े। जमाना जरा पुराना वाला था— “पढ़ऽ
पूत चंडिका,घर में चढ़े हंडिका” वाला।
“तीन पन्द्रहियें पंडित” की लोकोक्ति चलती थी।
अमरकोष, श्रुतबोध, लघुकौमुदी... होश सम्भालते ही रटा दिए जाते थे। प्रथमा-मध्यमा
पढ़े लोग भी विद्वानों में गिने जाते थे। फर्राटे से संस्कृत बोल लेते थे। आज की
तरह नहीं कि पीएच.डी. वाले को भी पीएच.डी.लिखने में तीन गलतियाँ निकल जायें।
मेरे
इस दावे को आप कृपया खारिज न करें, क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। एक बार
प्रयागराज, जिसे बदमिजाजियों ने इलाहाबाद नाम दे दिया है, एक सुपरिचित सज्जन से
मिलने गया था, उन्हें ताजी-ताजी मिली पीएच.डी. उपाधि की शुभकामना देने के ख्याल
से। शुभकामना स्वीकृति की औपचारिकता पूरी हुई। और फिर शुरू हो गई लगौंटिया यारी की
बातें। डिग्री लेने की मशक़्क़त से लेकर, बबुआ के ‘हैपी वर्थ डे’
तक के चुटीले-रसीले गपशप और
मिठाई का स्वाद चखने के बाद विदा होते समय अचानक मेरी खोजी आँखें अटक गई उनके
दरवाजे पर टंगी नई नाम-पट्टिका पर।
मुझे
गौर फरमाते देख, उन्होंने टोका।
मैंने
मुस्कुराते हुए जरा मज़ाकिया अन्दाज़ में कहा— पेन्टर की इस गलती को सुधरवा दो भाई
! लोग क्या सोचेंगे ! पीएच.डी. में एच स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल
नहीं। और ये पी के बाद वाला डॉट भी गलत ही है।
चट,
उनके चेहरे के भाव गवाही दे गए कि बात उन्हें बहुत लग गई। झल्लाते हुए तपाक से
बोले—तुम तो मैट्रिक का भी मुँह नहीं देखे और बात कर रहे हो पी..ऽ.ऽ ऽ ऽ एच... ऽ.ऽ.ऽ.ऽ
डी...ऽ ऽ ऽ ऽ की ? — कहते समय अभागे तीनों अक्षरों
की बहुत खिंचाई हुई थी, जिसका दर्द मुझे कभी-कभी शाल जाता है।
क्योंकि
उस मुलाकात के बाद नियमित पत्राचार वाला सिलसिला टूट गया। इत्तफ़ाकन एक बार
कुम्भस्नान में मुलाकात भी हुई तो, उनकी मुस्कान भी बड़ी मेहनती लगी मुझे।
खैर,
मैं बात कर रहा था बाबा वटेसरनाथ की। युवावस्था में ही बाबावटेसरनाथ अपने जन्म-स्थान
से पलायन कर, सुदूर पूर्वांचल की टोह में निकल गए थे, क्योंकि “पढ़ऽ पूत चंडिका,घर में चढ़े हंडिका” वाला दबाव झेलना उन्हें अच्छा नहीं लगा और “तीन
पन्द्रहियें पंडित” से तो श़ख्त नफ़रत थी उन्हें।
लम्बे
भटकाव के बाद इनका ठहराव और अटकाव हुआ महानगर कलकत्ता में। और फिर धीरे-धीरे वहीं
पैर पसारने की कवायद करने लगे।
पुराने
वाले कलकत्ते से सुपरिचित लोग भलीभाँति जानते हैं कि देश की पूर्वी सीमा पर स्थित
ये महानगर देशी ही नहीं, विदेशियों के लिए भी आकर्षण और लोभ का निवाला रहा है।
सुनते हैं कि फिरंगियों ने समुद्रीयात्रा का लंगर यहीं डाला था । ‘मुगलों
ने सल्तनत बक्श दी’ कहानी के लेखक ने इसी कलकत्ते में फिरंगियों का पहला
तम्बू गड़ने की बात कही है। वही तम्बू धीरे-धीरे खिंचते-खिंचाते, दिल्ली की सल्तनत
पर काबिज हुई थी, जिसका कुपरिणाम देश ने कई शताब्दियों तक झेला और अभी भी उस ‘झेलन’ की
छाप पूरी तरह से खतम नहीं हुई है।
यही वो कलकत्ता है, जहाँ देश का सबसे पहला वेश्यालय
बसाया गया फिरंगियों द्वारा। अपना हुकूमत फौलादी बनाने के ख्याल से देशवासियों में
से ही चाटुकार चन्द चुनिन्दों को मानिन्द बनाकर, देशवासियों पर ज्यादती करने का
जिम्मा सौंपा गया था—तरह-तरह की लुभावनी उपाधियाँ और सुविधाएँ दे देकर।
‘शान्तिनिकेतन’ तो
बहुत बाद में बना था, किन्तु अशान्ति का इमामबाड़ा बहुत पहले खड़ा कर दिया गया था।
भले ही अब ‘मुम्बादेवी’ वाली महानगरी रंगीन मिज़ाज़ियों के लिए बाकी शहरों के
कान काटने में अब्बल हो, किन्तु ‘सोनागाछी’ और
‘दालमंडी’ में
प्रतिस्पर्द्धा रहती थी उन दिनों । रायबहादुरों को ये दोनों जगहें बहुत प्यारी थी।
चुँकि बाबा वटेसरनाथ इन दोनों जगहों के बीच के वासिन्दे
थे, इसलिए जरुरत के मुताबिक ‘पैरेड’ करते रहते थे और वहाँ के
हुक्मरानों को नयी-नयी चिंड़िया के पंखों का रंग बतलाते रहते थे।
धीरे-धीरे
वावा वटेसरनाथ का भी रंग निखरता गया—चाँदी की चमक से। कहने वाले कहा करते हैं कि
चाँदी की जूती भी सिर पर पड़े तो सौभाग्य ही मनावें, यहाँ तो चाँदी की खनक थी
झोलियों में।
कुछ
ही वर्षों में बाबा का हाथ-पैर आसपास के टोले-टापुओं तक पसरने लगे। कोलम्बो,
सिंगापुर, ताईवान, वर्मा... यहाँ तक कि जर्मन-जापान तक परिचय-पहुँच बन गई।
ज्यादातर
झोलियाँ देश के बैंकों के वजाय टापुओं के बैंकों में रखी जाती। भाई कहीं हिस्सेदार
न बन जाए—के ख्याल से, ससुराल और समधियाने में कुछ जमीनें भी खरीदी गईं।
इसी
बीच काल ने करवट ली। लम्बी गुलामी के बाद देशवासियों ने आजादी की हवा में सांस ली।
किन्तु बाबा वटेसरनाथ पर दुर्दिन का पहाड़ टूट पड़ा। बाहरी बैंकों में जमा रकम
वहीं की वहीं ‘सीज’ हो गई किसी कारण वश। ढाका अब पूर्वी पाकिस्तान
बन गया। पता नहीं क्यों कलकत्ते का ‘रहनिहार’ ढाका के बैंकों को आबाद कर रहा था !
लोग
कहते हैं कि ‘सनिचरा’ आते हैं तो हाथी पर सवार को भी कुत्ता काट
लेता है...भूँनी मछली भी तालाब में कूद भागती है। बाबा वटेसरनाथ के साथ भी कुछ ऐसा
ही घटित हो गया।
सास-श्वसुर
हैजे की महामारी में चल बसे। समधीजी स्वर्ग तो नहीं सिधारे, किन्तु दो बेटों के
अधीन हो गए। परिणाम ये हुआ कि ससुराल और समधिआने में खरीदी गई बीसियों बीघा जमीन
से हाथ धोना पड़ा वावा वटेसरनाथ को। दरअसल आत्मीयता और विश्वास ने अपने नाम को भी
जमीनी कागजातों में जगह न दी थी। और ये बात भी सच ही है कि स्वतन्त्र भारत में घोर
बेईमानी की भी स्वतन्त्रता मिल गई बहुतों को। दोनों ग्रुप के साले भी उसी ग्रेड के
निकले।
नतीजा
ये हुआ कि वावा कोठी से कोठरी में सिमट गए कलकत्ते की गलियों में। भारत के एक दूरदर्शी सपूत की
बुद्धि-कौशल से रजवाड़े विलीन हो गए गणतन्त्रभारत में और ऐयाश़ जमींदारों की भी
कब्र खुदने लगी। ऐसे में अदने से मुखविरी-चमचागिरी वाले बाबा वटेसर नाथ की क्या
विसात
!
विशेष
पढ़े-लिखे योग्य होते तो कलकत्ते के मारवाड़ी समाज में काफी कदर होती। दुर्दिन
आते-आते भी टल जाता।
अच्छे-बुरे,
कुकर्म-सुकर्म, संस्कार-कुसंस्कार विहीन बाबा वटेसर नाथ ने धनोपार्जन का एक नया
तरीका निकाला। शुरु से ही अकेले रहने वाले वटेसरबाबा, ज्यादातर मैके में ही पड़ी
रहने वाली पत्नी को कलकत्ता ले आए।
विदित
हो कि मारवाड़ी समाज में जोडा-जोड़ी ब्राह्मण-पूजन-भोजन का रिवाज है प्रायः।
पूजा-पाठ, यज्ञ-कर्मकाण्ड में निपुण भले न हों, ब्राह्मण भोजन में तो निपुणता
अवश्य हासिल थी उन्हें।
महीने
के अठाइस दिन भोजन-व्यवस्था हो ही जाती किसी न किसी तरह। बचे दो दिन भी चैन से
गुजर जाते—सीधा-बारी तो मिलता ही था न !
एक
काम और करते थे बाबावटेसरनाथ—अवसर देख नीमतल्ला घाट पर, रोज वाले सफेद धोती-चादर
को छोड़कर, श्याम वस्त्र धारण कर सुबह-सुबह बैठ जाते दोनों प्राणी—प्रेतब्राह्मण
वेष में।
आप
जानते ही हैं कि श्राद्धीय एकादशाह के दिन तिल-दूध पीने का दक्षिणा चाँदी ही होता
है। अन्न-वस्त्र के साथ दो सिक्के भी हाथ लग जाते इस अभिनव कौशल से। धीरे-धीरे
बाबा का नया रोजगार भी फलने-फूलने लगा।
बाबा
का एकमात्र पुत्र भी था, जो बाबा की तरह ही सरस्वती का महान शत्रु था। किन्तु दैवकृपा
से बुद्धि बृहस्पति और शकुनि वाली थी। नतीजन, ‘धृतराष्ट्र’ की महात्वाकांक्षाओं पर अमल-पहल किया इकलौते पुत्र ने।
पुत्र
की बुद्धि और शरीर दोनों पुष्ट हों, इस उम्मीद से खुलेआम सम्भव न होते हुए भी,
चुपके से दूध में ‘श्वेतशालग्राम’
घोल कर पिलाया करते वटेसरबाबा ।
परिणामतः
पिता की आकांक्षाओं पर लगभग खरा उतरा युवा ’धूर्जटी’, जो आगे चलकर ‘शिवबूटी’ को ही अपने जीवन का
अभिन्न अंग बना लिया। कमाई तो अच्छी होती, किन्तु मित्र-मण्डली में ही खप जाती। आप
जानते ही होंगे कि जीवन के कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जिसकी पूर्ती अकेले अच्छी नहीं
लगती। आपने किसी गंजेड़ी को अकेले-अकेले देखा है दम लगाते?
चिलम जबतक चारों ओर घूमे नहीं, मजा ही नहीं आता। शायद ऐसी ही किसी बात पर कवि को
सूझी हों ये पंक्तियाँ—उत्सवे व्यसने चैव, दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे।
राजद्वारे श्मशाने च, यः तिष्ठति स बान्धवः।। व्यसन में भी जो साथ न छोड़े, असली
साथी वही है न ! और इतना ही क्यों? ये
भी तो कहा ही गया है —
“ भिक्षोः !
मांस निसेवनं प्रकुरुषे, किं तेन मद्यं बिना ।
मद्यं चापि तवप्रिय,
प्रियमहो वारांगनाभि: सह ॥
तासामर्थ्यरुचि: कुतस्तव धनम्,
द्यूतेन चौर्येण वा ।
द्यूतं
चौर्यपरिग्रहोपि भवत:, नष्टस्य कान्या
गति:॥”
( ‘अरे भिखारी, तुम मांस भी खाते हो?’ – ‘खाता तो हूँ, लेकिन शराब के
बिना उसे खाने में क्या मज़ा !’ – ‘तो
तुम्हें शराब भी प्रिय है?’ –‘प्रिय तो
है, लेकिन जब तवायफ़ों के साथ पियें तब । ’ – ‘ये शौक पूरा करने के लिए तुम्हें धन कहाँ से
मिलता है?’ – ‘जूआ खेलकर और चोरी करके।’
–‘तो तुम जूआ भी खेलते हो और चोरी भी करते हो?’
– ‘ जो आदमी एक बार गिर जाए, फिर उसकी और क्या गति ? ’ )
कुछ
ऐसा ही घटित हुआ था बाबा वटेसर-पुत्र धूर्जटि के साथ भी। अपनी कमाई तो ज्यादा हुई
ही नहीं कभी चिलम-चिखना-चमड़ी से,
बाप की रही-सही कमाई भी मटियामेट हो गई।
और
फिर ‘जेनेटिक ईंजीनियरिंग’ के अनुसार पिता की थोड़ी-बहुत
छाप तो पुत्र पर भी होनी ही चाहिए। धूर्जटि पुत्र त्रय भी कुछ-कुछ ऐसे ही धुरन्धर
निकले। सरस्वती से बैर की पुस्तैनी धरोहर आगे-आगे बढ़ती रही ।
किन्तु
हाँ, एक खास बात जरुर हुई—बच्चों के मामाओं ने बेईमानी सिर्फ खरीदी गई जमीन की की
थी, किन्तु सभी भाँजों के लिए कोइलवरी में अच्छी-खासी कमाऊ कुर्सी की प्रबन्ध कर दी
। फलतः तीन पीढ़ियों वाला कलकत्ता छूट कर कोइलवरी प्रसिद्ध हो गया अगली पीढ़ी के
लिए। और चारों ओर पसरे पड़े-गड़े कोयले की कालिमा के बीच तन-मन-विचारों की कालिमा
का भला क्या मोल !
सब के सब हीरे के मोल बिक रहे हैं अब, आधुनिक समृद्ध समाज में।
हरि
अनन्त हरि कथा अनन्ता । बाबा वटेसरनाथ की कथा से अब मुझे भी उब हो रही है। अतः
विराम चाहता हूँ। वैसे
भी ये श्री सत्यनारायण कथा तो है नहीं ।
— XXXXX
—
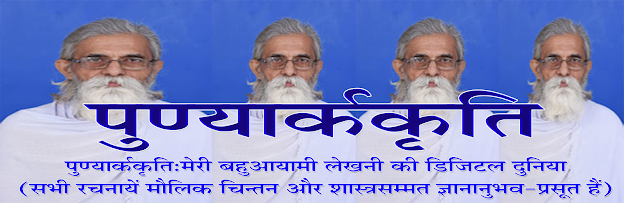
Comments
Post a Comment